दस महाव्रत [६]- शौच
Ten Mahavratas [6]- Cleanliness
SPRITUALITY
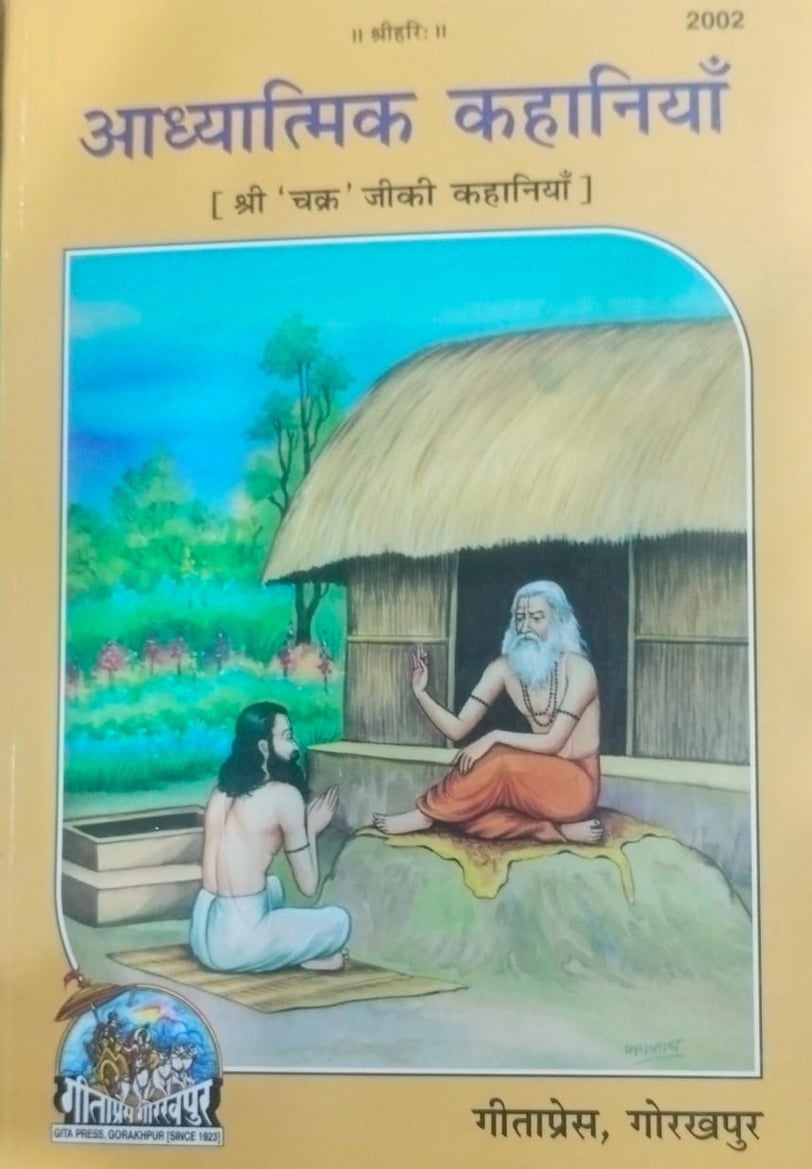
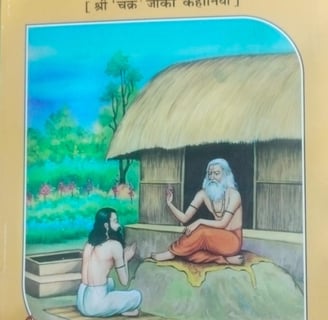
दस महाव्रत [६]-
शौच
(१)
'शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ।' *
* शौच (शुचिता) के पालनसे अपने अंगोंमें वैराग्य और दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है।
(योगदर्शन २।४०)
वह विचारक था। सम्भव नहीं था कि वह दूसरोंकी देखा-देखी एक छकड़ा सामान यों ही लादे-लादे फिरता। वैसे वह श्रद्धालु था और जिस दिनसे उसने रामानुज-सम्प्रदायकी दीक्षा ली, आचारसम्बन्धी प्रत्येक नियमका उसने अक्षरशः पालन किया। बिना कोई अपवाद निकाले, बिना कोई बहाना बनाये, वह नियमोंको बड़ी कठोरतासे निभाता था। दूसरे लोगोंके लिये वह आदर्श हो गया। फिर भी यह केवल कर्म-भार वह कबतक ढोता। वह विचारक था।
रमाकान्तने सोचना प्रारम्भ किया- 'दूसरोंकी दृष्टिमात्रसे मेरा भोजन अपवित्र हो जाता है। मेरे पात्र दूसरोंके स्पर्शके पश्चात् फिर अग्निसे भी शुद्ध नहीं होते। मेरे आसनपर कोई हाथ भी रख दे तो वह मेरे कामका नहीं। अन्ततः यह सब क्यों ? क्या श्रीमन्नारायणकी पूजाके निमित्त ? किंतु प्रभु तो प्रेमाधीन हैं। वे तो शूद्रोंपर भी प्रसन्न होते ही हैं। अविधि और विधि वहाँ केवल सच्ची प्रपत्ति है। तब क्या मैं दूसरोंसे अधिक पवित्र हूँ? लोग ऐसा कहते तो हैं; फिर भी क्या यह सत्य है?'
'दूसरोंसे मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ' - यह अहंकार ही तो गहन जाल है। रमाकान्त तन्मय था विचारोंमें, 'मेरे मनमें काम-क्रोधादि भरे हैं। मैं ही जानता हूँ कि मेरा मन कितना अशुद्ध है। रहा शरीर-हे भगवन् ! हड्डी, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, कफ, पित्त, थूक, मूत्र, मल, चर्म, केश प्रभृतिसे भरा यह शरीर !! इनमेंसे कोई भी छू जाय तो मुझे स्त्रान करना पड़ता है और मैं इन्हींको ढो रहा हूँ।'
शास्त्र और गुरुकी आज्ञा समझकर उसने नियमोंको शिथिल नहीं किया, पर अब उसे शरीरसे घृणा हो गयी। 'मैं शुद्धाचारी और पवित्र हूँ'- यह धारणा जाने कहाँ लुप्त हो गयी। जब वह शौचके पश्चात् हाथमें मिट्टी लगाता- 'उफ, यह रक्त और हड्डी क्या मलनेसे पवित्र होगी ?' भोजन बनाते समय जब पर्दा लगाकर वह भीतर बैठता-'छिः ! यह मांसका लोथड़ा तो चौकेमें ही है।' जब भोजन करने लगता- 'यह चर्म और नख मुखमें डाला जा रहा है! मुखमें ही क्या है? लार, अस्थि, चर्म !! भगवान्का प्रसाद समझकर भोजन कर लेता।'
शरीरसे उसे घृणा हो गयी। जिस शरीरके साज-शृङ्गारमें हम सब मरे जाते हैं; जिसे पुष्ट, नीरोग एवं निरापद रखनेके लिये जमीन-आसमान एक किया जाता है, उसे वह फूटी आँखों देखना नहीं चाहता था। विवश था उसे धारण करनेके लिये। आत्महत्या पाप जो है। 'ओह, यही अत्यन्त अशुद्ध और मलपूर्ण शरीर फिर धारण करना पड़ेगा ?' वह फूट-फूटकर रोने लगता था यह सोचकर ही। उसे इसी जीवनमें शरीर रखना पल-पल भारी हो रहा था।
(२)
माता-पिताका आग्रह था और रमाकान्त-जैसा श्रद्धालु उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता था। विवाह हो गया और पत्नी घर आयी। व्यर्थ ! भला, वह नितान्त एकान्त-प्रिय कहीं संतानोत्पादन कर सकता है।
'माताके उदरमें नौ महीने निवास- एक ओर मल, एक ओर मूत्र, कहीं पीब और कहीं रक्त। उस मांसकी थैलीमें रहना और फिर रक्त से लथपथ निकलना। एक जीवको मेरे कारण यह सब कष्ट-छिः !' वह इसकी कल्पनासे काँप जाता था। यों तो काम उसमें भी था, पर स्त्रीको देखते ही उसे दीखता था मांस, रक्त, अस्थि। वासना हवा हो जाती और घृणासे वह दूर भागता। जिसे अपने ही शरीरसे घृणा हो, वह दूसरेके शरीरको भला कैसे छू सकता है।
वह रोगी नहीं था और न कभी रोगने उसे दर्शन ही दिया। रोग तो होते हैं असंयमसे। जो भोजनमें रुचि न रखता हो, 'इसका बनेगा क्या ?' यह सोचकर भोज्य पदार्थोंसे घृणा करता हो, केवल प्रसाद समझकर, कुछ भगवान्को भोग लगाकर पेटमें डालता हो, - वह भी शुद्ध सात्त्विक, नपा-तुला, बालकी खाल निकाल-निकालकर जिसकी अशुद्धि दूर की गयी हो, ऐसे भोजनको ग्रहण करनेवालेके समीप रोगके आनेका मार्ग ही क्या है।
उसका काम क्या था ? दिनभर अपनी पवित्रताके खटरागमें और अपने लक्ष्मीनारायणकी पूजामें लगे रहना। दूसरोंका प्रभाव तो तब पड़े जब दूसरे पास जा सकें। दूसरोंकी वस्तुएँ भी तो बत्तीस बार धोकर प्रयोगमें आती थीं। अन्न-दोष, संग-दोष, स्थान-दोष, क्रिया-दोष-इनमेंसे किसीके फटकनेको स्थान ही न था। ऐसी स्थितिमें मनीरामका कल्याण प्रसन्न ही रहनेमें था। वे भी डरते थे कि कहीं अप्रसन्न हुआ और इन्होंने अपवित्र समझकर हमें भी थालीकी भाँति रगड़-रगड़कर माँजना-धोना प्रारम्भ किया तो पानीमें ही खोपड़ी सफाचट हो जायगी।
रूप- हड्डी, मांस, अस्थि आदि हैं- नेत्र बेचारे जहाँ जाते, वहीं घृणा और फटकार पड़ती। शब्द- कोई मांसका लोथड़ा पास है-कर्णका आनन्द मिट्टी हो जाता इस भावके आते ही। स्पर्श - राम ! राम !! चमड़ा छुयेगा। अरे ये फूल बने हैं मलकी खाद खाकर-सब गुड़ गोबर हो उठता त्वक्का। रस - क्या ? इनका परिणाम है मल और मूत्र और तब ये उससे भिन्न हैं। रसना बेचारी क्या करे। वमन करनेको जी चाहता था। गन्ध- नासिकाका सब मजा किरकिरा हो जाता, जब उसे बुद्धि खरी-खरी सुनाती कि ये सब गन्ध केवल मल-मूत्रसे पुष्ट हुई हैं या सड़कर नाबदान जैसी गन्ध देती हैं।
ज्ञानेन्द्रियोंकी तो यह दशा थी और कर्मेन्द्रियोंको धोने, इधरसे उधर करने, उठाने रखनेसे अवकाश ही नहीं था। वे करें तो क्या ? तनिक किसी कार्यमें विलम्ब होनेपर सबमें देर होने लगती। मनीराम फटकारने लगते; क्योंकि रमाकान्तजी तो सब कार्य तिल-तिल पूरा करेंगे और फलतः मनीरामजीका रात्रि विश्राम मारा जायगा। इसलिये इन्द्रियोंके तनिक भी प्रमाद करनेपर वे लाल-पीले होने लगते। वे बेचारी बसमें न रहें तो जायें कहाँ ?
(३)
'ओह, फिर स्नान करना होगा! सो भी इस शीत-कालमें। लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते कि जूतेको मार्गसे तनिक दूर उतारा करें।' रमाकान्त स्नान करके आ रहे थे। द्वारके समीप ही किसीने जूता उतार दिया था। वह पैरको लग गया। उन्हें तनिक खेद हुआ। सर्दीके मारे हाथ-पैर अकड़े जा रहे थे। 'प्रमाद तो मेरा ही है, मुझे देखकर चलना चाहिये।' वे वहींसे चल पड़े और पुनः स्नान करके आये। पूजा जो अभी शेष थी।
पूजा समाप्त हुई। प्रसाद अपने हाथ ही प्रस्तुत करना था। पात्रमें चूल्हेपर चावल सिद्ध होने लगा और रमाकान्तजी पास बैठे अपनी विचारधारामें तल्लीन हो गये। 'यह शरीर- इसका निर्माण ही समस्त अपवित्र वस्तुओंसे हुआ है और इसे पवित्र करनेके लिये इतना प्रयास ! क्या यह कभी शुद्ध हो सकता है? तब यह प्रयास क्यों होता है ?'
जूतेके स्पर्शका स्मरण हो आया- 'चमड़ेका जूता और उसके स्पर्शसे शरीर अपवित्र हो गया! क्यों? शरीर क्या उससे भी गंदे चमड़ेसे नहीं बना है? तब यह पवित्रता किसके लिये है! शरीरका क्या पवित्र और क्या अपवित्र होना। यह सब है आत्मशुद्धिके निमित्त । किंतु यह आत्मा है क्या ? जिसकी शुद्धिके लिये रात-दिन एक करना पड़ता है, वह आत्मा शरीरके भीतर ही तो है!'
जैसे बिजली छू गयी हो-'जरा-से मृतक-चर्मके स्पर्शसे तो यह शरीर अपवित्र हो गया और जो आत्मा शरीरके भीतर इस मज्जा-मांसमें ही रहता है, वह कैसे शुद्ध होगा?' हृदयपर एक कठोर ठेस लगी। वे गम्भीर चिन्तामें तल्लीन हो गये। इतने तल्लीन कि चावल जलकर भस्म हो गया, पर उन्हें कुछ पता नहीं।
रमाकान्तजी विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे। थोड़ी हिन्दी और काम चलानेभरको संस्कृत जानते थे। उसीसे विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके कुछ ग्रन्थ पढ़ लेते थे। वैसे उन्हें पढ़नेका अवकाश भी कहाँ था। अपनी ही पद्धतिसे वे सोच रहे थे- 'यदि आत्मा शरीरमें ही रहता है तो कहाँ रहता है! उसका स्थान हृदय बतलाया गया है, तब क्या रक्तपूर्ण हृदयमें वह रक्तसे लथपथ है!'
उन्होंने हृदयमें मनको एकाग्र किया। इन्द्रियोंको थोड़ी शान्ति मिली, इस बराबर धोने-माँजनेकी खटपटसे। मनीराममें इतनी शक्ति ही न थी, जो इधर-उधर कर सकें। उन्हें तो आज्ञापालन करना था; क्योंकि बराबरकी स्वच्छताने उन्हें भी झाड़-पोंछकर स्वच्छ कर दिया था। बाहरी शुद्धि मन शुद्ध करनेमें हेतु होती ही है और मन शुद्ध होनेपर इस प्रकार अपने ही अङ्गोंमें अपवित्रताका बोध होना स्वाभाविक है!
'हृदय है-छिः यह भी मांसका ही है! इसके भीतर है रक्त। अति अपवित्र रक्त !! इसके और भीतर - अन्तस्तलमें ? हृदयाकाश-विशुद्ध प्रकाशमय हृदयाकाश !!!' बस ! इसके पश्चात् मनीराम पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गये। वे भगे नहीं, उनकी सत्ता ही लुप्तप्राय हो गयी। रमाकान्तजी स्थिर, अविचल, शान्त बैठे थे।
दिन गया, रात्रि आयी और वह भी चली गयी। 'प्रातःकाल आज रमाकान्त चरणस्पर्श भी करने नहीं आया ? सर्दीमें भी वह दिनभर पानीमें हाथ डाले रहता है। उसे स्नान और संध्या ही दिनभर लगी रहती है। कहीं सर्दी तो नहीं लग गयी?' माताका ममत्व आर्द्र हो उठा। रमाकान्तजीके एकान्तमें कोई बाधा न पड़े, इसलिये कोई उनके पास नहीं जाता था। वे प्रायः दूसरे घेरेवाली कोठरीमें अकेले रहते थे। माता उधर गयीं। द्वार खुला पड़ा था, चूल्हेपर पात्र रखा था, अग्निके बदले कुछ भस्म थी और रमाकान्त आसनपर बैठे थे।
माताने पुकारा, बहुत पुकारनेपर भी जब वे न बोले तो स्पर्श किया- 'शरीर शीतल, जैसे हिम! नासिकाके पास हाथ ले जानेपर भी श्वासकी गति प्रतीत नहीं होती!' माता चीख पड़ीं। भीड़ लग गयी और बहुत चिल्लाहट हुई। थोड़ी देरमें श्वास चला, शरीरमें थोड़ी उष्णता आयी और रमाकान्तजीने नेत्र खोल दिये।
'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' रमाकान्त पूर्णतः बदल गये थे। अब न शरीरका पता रहता था और न संसारका। जब मौज आती तो उपर्युक्त वाक्य कहते और हँस पड़ते। इसके सिवा उन्हें कोई कार्य न था।
